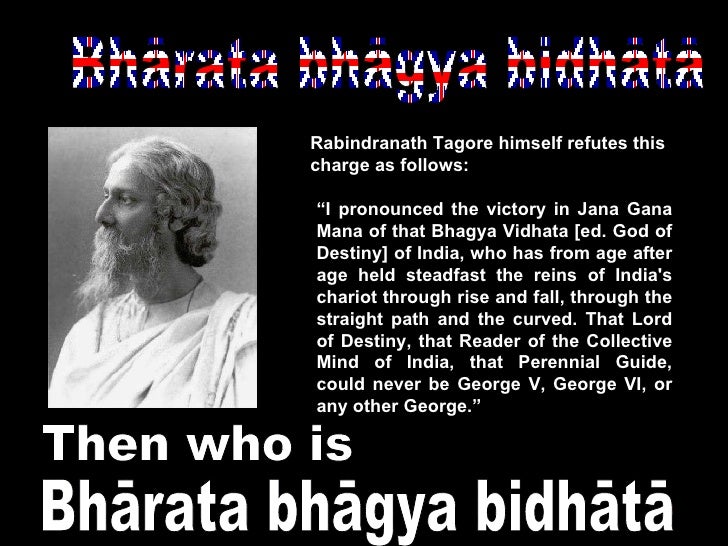[आज ईद के मौके पर देवी प्रसाद मिश्र की "मुसलमान" कविता "स्वाधीन" के पाठकों के लिए पेश है, इस कविता को पढ़कर जानिए कि मुसलमानों का इस देश के निर्माण में क्या खून- पसीना लगा है... और कैसे ये फुफकारते यवन सांप' इस देश का हिस्सा बन गए...]

देवी प्रसाद मिश्र
मुसलमान
कहते हैं वे विपत्ति की तरह आए
कहते हैं वे प्रदूषण की तरह फैले
वे व्याधि थे
ब्राह्मण कहते थे वे मलेच्छ थे
वे मुसलमान थे
उन्होंने अपने घोड़े सिन्धु में उतारे
और पुकारते रहे हिन्दू! हिन्दू!! हिन्दू!!!
बड़ी जाति को उन्होंने बड़ा नाम दिया
नदी का नाम दिया
वे हर गहरी और अविरल नदी को
पार करना चाहते थे
वे मुसलमान थे लेकिन वे भी
यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए तो
हिन्दुओं की तरह पैदा होते थे
उनके पास बड़ी-बड़ी कहानियाँ थीं
चलने की
ठहरने की
पिटने की
और मृत्यु की
प्रतिपक्षी के ख़ून में घुटनों तक
और अपने ख़ून में कन्धों तक
वे डूबे होते थे
उनकी मुट्ठियों में घोड़ों की लगामें
और म्यानों में सभ्यता के
नक्शे होते थे
न! मृत्यु के लिए नहीं
वे मृत्यु के लिए युद्ध नहीं लड़ते थे
वे मुसलमान थे
वे फ़ारस से आए
तूरान से आए
समरकन्द, फ़रग़ना, सीस्तान से आए
तुर्किस्तान से आए
वे बहुत दूर से आए
फिर भी वे पृथ्वी के ही कुछ हिस्सों से आए
वे आए क्योंकि वे आ सकते थे
वे मुसलमान थे
वे मुसलमान थे कि या ख़ुदा उनकी शक्लें
आदमियों से मिलती थीं हूबहू
हूबहू
वे महत्त्वपूर्ण अप्रवासी थे
क्योंकि उनके पास दुख की स्मृतियाँ थीं
वे घोड़ों के साथ सोते थे
और चट्टानों पर वीर्य बिख़ेर देते थे
निर्माण के लिए वे बेचैन थे
वे मुसलमान थे
यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है
तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए
कि वे प्रायः इस तरह होते थे
कि प्रायः पता ही नहीं लगता था
कि वे मुसलमान थे या नहीं थे
वे मुसलमान थे
वे न होते तो लखनऊ न होता
आधा इलाहाबाद न होता
मेहराबें न होतीं, गुम्बद न होता
आदाब न होता
मीर मक़दूम मोमिन न होते
शबाना न होती
वे न होते तो उपमहाद्वीप के संगीत को सुननेवाला ख़ुसरो न होता
वे न होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन होनेवाला कबीर न होता
वे न होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहनेवाला ग़ालिब न होता
मुसलमान न होते तो अट्ठारह सौ सत्तावन न होता
वे थे तो चचा हसन थे
वे थे तो पतंगों से रंगीन होते आसमान थे
वे मुसलमान थे
वे मुसलमान थे और हिन्दुस्तान में थे
और उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में थे
वे सोचते थे कि काश वे एक बार पाकिस्तान जा सकते
वे सोचते थे और सोचकर डरते थे
इमरान ख़ान को देखकर वे ख़ुश होते थे
वे ख़ुश होते थे और ख़ुश होकर डरते थे
वे जितना पी०ए०सी० के सिपाही से डरते थे
उतना ही राम से
वे मुरादाबाद से डरते थे
वे मेरठ से डरते थे
वे भागलपुर से डरते थे
वे अकड़ते थे लेकिन डरते थे
वे पवित्र रंगों से डरते थे
वे अपने मुसलमान होने से डरते थे
वे फ़िलीस्तीनी नहीं थे लेकिन अपने घर को लेकर घर में
देश को लेकर देश में
ख़ुद को लेकर आश्वस्त नहीं थे
वे उखड़ा-उखड़ा राग-द्वेष थे
वे मुसलमान थे
वे कपड़े बुनते थे
वे कपड़े सिलते थे
वे ताले बनाते थे
वे बक्से बनाते थे
उनके श्रम की आवाज़ें
पूरे शहर में गूँजती रहती थीं
वे शहर के बाहर रहते थे
वे मुसलमान थे लेकिन दमिश्क उनका शहर नहीं था
वे मुसलमान थे अरब का पैट्रोल उनका नहीं था
वे दज़ला का नहीं यमुना का पानी पीते थे
वे मुसलमान थे
वे मुसलमान थे इसलिए बचके निकलते थे
वे मुसलमान थे इसलिए कुछ कहते थे तो हिचकते थे
देश के ज़्यादातर अख़बार यह कहते थे
कि मुसलमान के कारण ही कर्फ़्यू लगते हैं
कर्फ़्यू लगते थे और एक के बाद दूसरे हादसे की
ख़बरें आती थीं
उनकी औरतें
बिना दहाड़ मारे पछाड़ें खाती थीं
बच्चे दीवारों से चिपके रहते थे
वे मुसलमान थे
वे मुसलमान थे इसलिए
जंग लगे तालों की तरह वे खुलते नहीं थे
वे अगर पाँच बार नमाज़ पढ़ते थे
तो उससे कई गुना ज़्यादा बार
सिर पटकते थे
वे मुसलमान थे
वे पूछना चाहते थे कि इस लालकिले का हम क्या करें
वे पूछना चाहते थे कि इस हुमायूं के मक़बरे का हम क्या करें
हम क्या करें इस मस्जिद का जिसका नाम
कुव्वत-उल-इस्लाम है
इस्लाम की ताक़त है
अदरक की तरह वे बहुत कड़वे थे
वे मुसलमान थे
वे सोचते थे कि कहीं और चले जाएँ
लेकिन नहीं जा सकते थे
वे सोचते थे यहीं रह जाएँ
तो नहीं रह सकते थे
वे आधा जिबह बकरे की तरह तकलीफ़ के झटके महसूस करते थे
वे मुसलमान थे इसलिए
तूफ़ान में फँसे जहाज़ के मुसाफ़िरों की तरह
एक दूसरे को भींचे रहते थे
कुछ लोगों ने यह बहस चलाई थी कि
उन्हें फेंका जाए तो
किस समुद्र में फेंका जाए
बहस यह थी
कि उन्हें धकेला जाए
तो किस पहाड़ से धकेला जाए
वे मुसलमान थे लेकिन वे चींटियाँ नहीं थे
वे मुसलमान थे वे चूजे नहीं थे
सावधान!
सिन्धु के दक्षिण में
सैंकड़ों सालों की नागरिकता के बाद
मिट्टी के ढेले नहीं थे वे
वे चट्टान और ऊन की तरह सच थे
वे सिन्धु और हिन्दुकुश की तरह सच थे
सच को जिस तरह भी समझा जा सकता हो
उस तरह वे सच थे
वे सभ्यता का अनिवार्य नियम थे
वे मुसलमान थे अफ़वाह नहीं थे
वे मुसलमान थे
वे मुसलमान थे
वे मुसलमान थे.