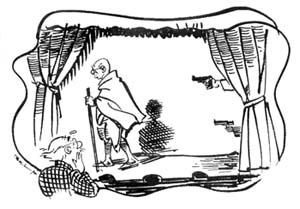आतिफ रब्बानी
समयांतर
[मनरेगा क्रोनी कैपिटलिज्म का पहला निशाना क्यों बना? क्योंकि यह देश के सबसे गरीब तबके को फायदा पहुँचाने वाली योजना थी। "मनरेगा का अर्थशास्त्र" में आतिफ रब्बानी ने खूब समझाया है कि मनरेगा क्यों जरूरी है। समयांतर में प्रकाशित इस लेख को स्वाधीन पर पुनर्प्रकाशित करना जरूरी लगा। जरूर पढ़िए...]
अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स—जिसे उन्नीसवीं सदी के मशहूर विक्टोरियाई इतिहासकार टॉमस कार्लाइल ने ‘डिसमल साइन्स’ की संज्ञा दी थी—भी अजीब और कन्फ्यूजिंग विषय है! अल्फ्रेड मार्शल से लेकर ग्रेगरी मैनकीव तक, एडमंड फ़ेल्प्स से लेकर जोन रॉबिंसन तक, मिल्टन फ्रिडमैन से लेकर पॉल सैमुएल्सन तक—जितने अर्थशास्त्री उतने सिद्धांत। अमेरिकी अर्थशास्त्री एडगर फीडलर ने लिखा था—“आप किसी विषय पर पांच अर्थशास्त्रीयों से बात कीजिए, आपको पांच अलग-अलग जवाब मिलेंगे। और अगर उनमें कोई हार्वर्ड का पढ़ा हो तो वह ख़ुद दो तरह के जवाब देगा। यानी पांच अर्थशास्त्री, छह जवाब।” लगभग ऐसा ही दृश्य आज भारत के अर्थशास्त्रियों के बीच दिखता है। जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के भविष्य को लेकर देश के 28 प्रमुख अर्थशास्त्री—जिनमें ज्यां द्रेज़, ऋतिका खेरा, अभिजीत सेन, जयंती घोष और अश्विनी देशपांडे आदि प्रमुख हैं—ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमे इसके ख़त्म किए जाने का ख़दशा ज़ाहिर किया गया और पत्र में इस योजना को आगे भी जारी रखने की गुज़ारिश की गयी। तो वहीं ‘सरकारी’ अर्थशास्त्रियों का एक समूह—जिसमें अरविंद सुब्रमण्यन, जगदीश भगवती और अरविंद पनगढ़िया आदि हैं—का मानना है कि नरेगा के दायरे को सीमित कर दिया जाना चाहिए और, अगर हो सके तो, अंततः इसको समाप्त भी किया जा सकता है। मतलब, योजना को लेकर विभिन्न अर्थशास्त्रियों के बीच भारी मतांतर है। बहरहाल, जैसा कि लियोनेल रोबिंसन ने कहा है कि अर्थशास्त्र, सीमित संसाधनों और उनके प्रयोग के मध्य अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन है। लिहाज़ा, मनरेगा के बजट (संसाधन) और इसके कार्यान्वयन (प्रयोग) के आईने में इसकी पड़ताल करते हैं कि क्या योजना भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही है? क्या देश में वित्तीय संसाधनों का इतना टोटा है कि इस योजना को अब और आगे जारी नहीं रखा जा सकता? क्या इस योजना को यूं ही समेट दिया जाना चाहिए?
क्या है मनरेगा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 की शुरुआत 2 फरवरी, 2006 को ग्रामीण क्षेत्रों में की गई। इसका मक़सद ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत हर परिवार के एक वयस्क सदस्य को एक साल में कम से कम 100 दिनों का रोज़गार दिए जाने की गारंटी है। इसका एक लक्ष्य टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन करना भी है। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े ज़िलों में लागू किया गया। दूसरे चरण में वर्ष 2007-08 में इसमें 130 और ज़िलों को शामिल किया गया, जबकि एक अप्रैल 2008 से इसका विस्तार सभी शेष ग्रामीण ज़िलों तक कर दिया गया। इसका आधार अधिकार और मांग को बनाया गया, जिसकी वजह से यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसके तहत समयबद्ध रोजगार गारंटी और 15 दिनों के भीतर मज़दूरी का भुगतान करना आदि शामिल है। इसका 90 फीसदी खर्च केंद्र सरकार वहन करती है, इसलिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रोज़गार प्रदान करने में कोताही न बरतें। इसके अलावा इस बात पर भी ज़ोर दिया जाता है कि रोज़गार शारीरिक श्रम आधारित हो, जिसमें ठेकेदारों और मशीनों का कोई दखल न हो। इसमें महिलाओं की 33 फीसदी श्रम भागीदारी सुनिश्चित की गई है। श्रम मद में 40 फीसदी और सामग्री मद में 60 फीसदी खर्च किए जाने की अधिकतम सीमा तय की गई है। पहले इसका नाम नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना था। बाद में इसका नाम बदल कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना किया गया।
ग़ौरतलब है कि कृषि क्षेत्र में भारी मात्र में अधिशेष श्रम है। एक ओर जहां देश के जीडीपी में कृषि का योगदान 15 फीसदी से कम है वहीं कुल श्रमशक्ति का तकरीबन 50 फीसदी हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है। जो लोग इस क्षेत्र से निकल भी गए हैं उनके लिए भी शहरी रोजगार क्षेत्र बहुत उत्साहित करने वाला नहीं है। इस कार्य शक्ति का 40 फीसदी स्वरोजगार वाला है जबकि अन्य 18 फीसदी अंशकालिक श्रमिक हैं। सरकारी क्षेत्र समेत समूचा संगठित क्षेत्र कुल कर्मचारियों के महज 7 फीसदी के लिए ही जिम्मेदार है। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोग सामाजिक सुरक्षा के कवच से बाहर हैं—यह एक अलग कहानी है। आर्थिक वृद्धि ही नहीं, सामाजिक तानेबाने को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि किसी न किसी तरह से इस अधिशेष श्रम को उपयोगी बनाया जाय। निश्चित ही, ऐसी स्थिति में नरेगा एक कारगर नुस्ख़ा है।
मनरेगा पर गिरती गाज
केंद्र की मोदी सरकार मनरेगा का दायरा सिकोड़ना चाहती है। पूरे देश में चल रही इस योजना को मौजूदा सरकार महज जनजातीय या पिछड़े जिलों तक ही सीमित करना चाहती है। साथ ही, सरकार की योजना मनरेगा एक्ट में संशोधन कर इसमें वर्णित श्रम और सामग्री के मौजूदा अनुपात (60:40 से घटा कर 51:49) को बदलने की है। इस दिशा में, सरकार ने राज्यों से यह कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के शेष महीनों में वे मनरेगा पर अपना खर्च सीमित करें।
उल्लेखनीय है कि अधिकार आधारित इस योजना की मद में किया जाने वाला बजटीय आवंटन पिछले कई वर्षों से लगातार कम हो रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए मनरेगा के मद में आवंटन महज 34,000 करोड़ रुपये का है, जो राज्यों द्वारा इस मद में मांगी गयी राशि से 45 प्रतिशत कम है (देखें तालिका-1)। जहां तक मनरेगा-जीडीपी अनुपात की बात है, वर्ष 2009-10 में देश की जीडीपी में मनरेगा के मद में हुए आवंटन का हिस्सा 0.87 प्रतिशत था, जो 2013-14 में घट कर 0.59 प्रतिशत हो गया। मनरेगा के अंतर्गत खर्च की गयी राशि का सालाना औसत 38 हजार करोड़ रुपये का रहा है, जबकि सालाना आवंटन औसतन 33 हजार करोड़ रुपये का हुआ है।
तालिका-1: नरेगा में व्यय की प्रवृत्ति
वर्ष कुल व्यय (करोड़ रु)
2009-10 37545
2010-11 39400
2011-12 37787
2012-13 39660
2013-14 38598
स्रोत: बजट दस्तावेज़ (विभिन्न वर्ष)
अगर सरकार मनरेगा को संकुचित करने के प्रस्तावित एजेंडे पर अमल-दर-आमद न करे तब भी मुद्रास्फीति के बढ़ने और आवंटित राशि की कमी के दोतरफा दबाव में मनरेगा का क्रियान्वयन लगातार बाधित होता रहा है। आवंटन में हो रही कमी को ध्यान में रखें, तो समझ में आता है कि सौ दिन की जगह क्यों अभी तक मनरेगा में गरीब ग्रामीण परिवारों को सालाना औसतन 50 दिन का भी रोजगार नहीं दिया जा सका। मनरेगा के अंतर्गत 2013-14 में कुल 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। वहीं, अगर श्रम और सामाग्री पर खर्च की जानेवाली राशि का अनुपात बदला जाता है—60:40 से घटा कर 51:49 किया जाता है—तो मनरेगा के अंतर्गत रोजगार-सृजन की मौजूदा दर कायम रखने के लिए अतिरिक्त 20 हजार करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी। चूंकि सरकार मनरेगा का बजट आवंटन बढ़ाने की जगह घटा रही है, तो इस का सीधा प्रभाव यह पड़ेगा कि मनरेगा के रोजगार सृजन की क्षमता में 40 प्रतिशत की कमी आयेगी। वहीं अगर श्रम-सामग्री अनुपात घटाने के साथ-साथ नरेगा को 200 पिछड़े जिलों तक महदूद किया जाता है तो ढाई करोड़ परिवार प्रभावित होंगे (तालिका-2)।
तालिका-2: 2013-14 के नरेगा आंकड़े
कुल नरेगा व्यय (श्रम+सामाग्री) (करोड़ रु.) 36228.7
200 पिछड़े जिलों में कुल नरेगा व्यय (श्रम+सामाग्री) (करोड़ रु.) 16890.17
200 पिछड़े जिलों में श्रम के दिन (करोड़) 87.12
200 पिछड़े जिलों में परिवार को मिला रोजगार (करोड़) 2.014
श्रम-सामग्री अनुपात घटाने (51:49) पर 200 पिछड़े जिलों में श्रम के दिन (करोड़) 64.913
श्रम-सामग्री अनुपात घटाने पर 200 पिछड़े जिलों परिवार को मिला रोजगार (करोड़) 1.501
मनरेगा का दायरा सिकोड़ना पर प्रभावित परिवार (करोड़) 2.479
स्रोत: http://nrega.nic.in/
बेकार का तर्क
मनरेगा के विरोध में प्रबल तर्क है कि इस योजना से राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है और देश की अर्थ व्यवस्था इस स्थिति में नहीं कि वह इतना वित्तीय भर सहन कर सके। आइए, इस तर्क पर ग़ौर करते है कि क्या वास्तव में देश पास इतने वित्तीय संसाधन नहीं जिससे इस योजना को जारी रखा जा सके?
नव-उदारवादी और नव-शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों को संख्याओं, अर्थमितीय, गणितीय और सांख्यिकीय पद्धतियां बहुत आकर्षित करती हैं। आमजन को सांख्यिकीय पद्धति के बारे में, गणितीय दांव पेंच और आंकड़ों की बाज़ीगरी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। ऐसा अमूमन समझा जाता है कि सांख्यिकीय आंकड़ों के ज़रिये पेश किया गया मफ़रूज़ा सैक्रोसैन्क्ट है—उसमे किसी भी प्रकार के बहस की कोई गुंजाइश नहीं। जबकि, हक़ीक़त इसके उलट होती है। वे सिर्फ़ सिक्के का एक रुख़ दिखाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला मनरेगा के खिलाफ दिये जाने वाले तर्क का है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि मनरेगा से राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। यह सिर्फ़ सिक्के का एक रुख़ है। दूसरे रुख़ की तरफ भी ज़रा ग़ौर करिए, मनरेगा का बजट जीडीपी का केवल 0.3 प्रतिशत है, जबकि अमीर कंपनियों को कर में जो छूट मिलती है, वह जीडीपी का तीन प्रतिशत है। मतलब साफ है—जितना मनरेगा पे ख़र्च किया जा रहा है उससे दस गुना ज़्यादा पैसा तो अमीरों को छूट देने मे ख़र्च हो रहा है। नरेगा कोई बहुत महंगी योजना नहीं है। पिछले वित्त वर्ष में, नरेगा के लिए कुल व्यय मात्र 38,598 करोड़ रुपए था।
ऐसा नहीं कि भारत ही सिर्फ़ एक ऐसा देश है जो मनरेगा पर इतना व्यय कर रहा है। लातिन अमेरिकी देश भी अपने-अपने देशों में ग़रीबी उन्मूलन, रोज़गार सृजन समेत स्वास्थ्य के विभिन्न कार्यक्रमों में में अपने जीडीपी का अच्छा-ख़ासा हिस्सा व्यय कर रहे हैं। मसलन, ब्राज़ील ‘बॉल्सा फ़ेमेलिया’ और मेक्सिको ‘अपार्चुनिदादिस’—जो ग़रीबी उन्मूलन व रोज़गार सृजन से संबन्धित कार्यक्रम हैं—में क्रमशः 0.3 और 0.5 प्रतिशत व्यय कर रहे हैं (तालिका-3)।
तालिका-3: ग़रीबी उन्मूलन कार्यकर्मों की लागत
लागत-जीडीपी अनुपात
बॉल्सा फ़ेमेलिया (ब्राज़ील) 0.3
अपार्चुनिदादिस (मेक्सिको) 0.5
नरेगा (भारत) 0.3
स्रोत: वर्ल्ड बैंक (एमएफ़डीआर प्रिन्सिपल्स इन एक्शन: सोर्सबुक ऑन एमर्जिंग गुड प्रैक्टिसेस)
यहाँ तक कि भारत सामाजिक सेवाओं पर भी लैटिन अमेरिकी, उप-सहारा और पूर्व एशियाई देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम खर्च करता है। नवीनतम विश्व विकास संकेतक (वर्ल्ड डेव्लपमेंट इंडिकेटर्स) के अनुसार, पूर्व एशियाई देश अपने जीडीपी का 7.20 प्रतिशत, लैटिन अमेरिकी देश 8.5 प्रतिशत और उप-सहारा अफ्रीकी देश 7 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य और शिक्षा में खर्च करते हैं। और जहां तक सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, इस पैमाने पर भी भारत अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के मुक़ाबले काफी पीछे है। देश सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 1.70 प्रतिशत हिस्सा सोश्ल सेक्युरिटी पर ख़र्च करता है जो कि निम्न-मध्यम आय वाले एशियाई देश (3.4 प्रतिशत) के मुक़ाबले आधी और चीन (5.4 प्रतिशत) से एक तिहाई से भी कम है। यह यूं ही नहीं है कि इन लातिनी अमेरिकी देशों का मानव विकास सूचकांक भारत से ज़्यादा है।
मनरेगा का 105 साल का ख़र्च
अब सवाल उठता है कि क्या वाक़ई भारत के पास इतने वित्तीय संसाधनों की कमी है कि नरेगा जैसी योजनाओं को आगे जारी रखा जा सकता? जवाब है, बिलकुल नहीं। भारत में कंपनियों को तो इतनी छूट दी जा रही है जिससे मनरेगा का 1 नहीं 105 साल का ख़र्च निकाल सकता है।
मशहूर लेखक और वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने अपने अध्ययन में खुलासा किया कि सरकार ने पिछले नौ सालों में कंपनियों को 365 खरब रुपए की टैक्स छूट दी है। इसका एक बड़ा हिस्सा तो हीरे और सोने जैसी चीज़ों पर टैक्स छूट में दिया गया। साईनाथ का कहना है कि सरकार अगर ये रक़म टैक्स छूट में नहीं देती तो इससे लंबे समय तक मनरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ख़र्च उठाया जा सकता था। इस साल के बजट के दस्तावेज़ों के मुताबिक़ हमने 2013-14 में ज़रूरतमंद कॉर्पोरेट और अमीरों को 5.32 लाख करोड़ रूपए दे दिए। इस 5.32 लाख करोड़ रूपए से 105 साल तक मनरेगा की योजना बड़े आराम के साथ चलायी जा सकती है।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन और ज्यां द्रेज़ ने भी अपनी किताब एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शन्स में इस विसंगति (एनॉमली) की तरफ़ इशारा किया है कि भारत का सब्सिडी ढांचा कितना पक्षपातपूर्ण है। जहां पैसे की ज़रूरत वहाँ तो मितव्यययिता से काम चलाया जा रहा है जबकि, गैरज़रूरी क्षेत्रों में बिलादरेग़ पैसे ख़र्च किए जा रहे हैं। कमी संसाधनों की नहीं, प्राथमिकताओं में है।
अफसोस की बात है कि सरकार संसाधनों की कमी का रोना तो रोती है लेकिन सरकारी आय बढ़ाने पर चर्चा बिलकुल महीन करती। इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई पुस्तक कैपिटल इन द ट्वेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी के लेखक अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी और नैन्सी कियान की शोध रिपोर्ट ‘इनकम इनएक्वालिटी एंड प्रोग्रेसिव इंकम टैक्सेशन इन चाइना एंड इंडिया, 1986-2015’ के अनुसार, 1986 से 2008 के बीच चीन में कर देने वाली जनसंख्या 0.1 से बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि इस दौरान भारत मे यह दो से तीन प्रतिशत के बीच अटकी हुई है।
एक फ़र्सूदा तजवीज़
मनरेगा विरोध में पेश-पेश नव-उदारवादी/नव-शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों का ख़ेमा अमेरिकी नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. एडमंड फेल्प्स के उस व्यक्तव्य से प्रभावित है जिसमें उन्होने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता और रोज़गार सृजन व गारंटी जैसे कार्यक्रमों के बजाय रोजगार सबसिडी देनी चाहिए। इससे बड़े उद्यमों के लिए श्रमिकों को रोजगार देना सस्ता हो जाएगा और कॉमर्शियल रोजगार में भी वृद्धि होगी। दी गई रकम की आंशिक वसूली बढ़ी हुई कॉमर्शियल गतिविधि से हो जाएगी। श्रम सस्ता होने के कारण उद्यमों की लागत कम आएगी, वे उत्पादन ज्यादा करेंगे और टैक्स ज्यादा अदा करेंगे। हो सकता है कि यह तर्क अमेरिका के संदर्भ में सही हो, लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है यहाँ तो ऐसा होने से रहा है। कौन नहीं जानता कि पिछले दो दशकों में बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों पर सरकार ने पैसे पानी की तरह लुटाए हैं—करों में छूट, सबसिडी, कौड़ी के भाव ज़मीनों का देना सहित वे तमाम तरीके हैं जिसके ज़रिये बड़े औद्योगिक घरानों को लाभान्वित किया गया है। मगर नतीजा वही ढाक के तीन पात—संगठित रोज़गार में वृद्धि के बजाए ह्रास हुआ है।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएस) के 68 वें राउंड के आंकड़ों तो कम से कम यही दिखाते हैं। इन आंकड़ों के अनुसार जून, 2010 से जून, 2012 के बीच बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। पिछले दो साल के दौरान देश में बेरोजगारी 10.2 फीसदी की दर से बढ़ी है। इन आंकड़ों के मुताबिक़ जनवरी, 2012 में देश में पूर्ण बेरोजगारों की संख्या 1.08 करोड़ थी, जबकि दो साल पहले यह आंकड़ा 98 लाख था। इन आंकड़े के अलावा कई सरकारी एवं गैरसरकारी सर्वेक्षणों के आंकड़े भी बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारी की बात कह रहे हैं।
इससे पूर्व एनएसएस के 66 वें राउंड के अनुसार, वर्ष 2004-05 और 2009-10 के बीच रोज़गार में सालाना 0.8 प्रतिशत की ही बढ़ोत्तरी हुई जबकि जनसंख्या की वृद्धि दर 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। जनसंख्या वृद्धि दर और रोज़गार दर की इस असंगति से बहुत कम ही लोगों को नियमित क्षेत्र में रोजगार मिलता है बाक़ी लोग असंगठित क्षेत्र का हिस्सा बन जाते है। इस तरह साल-दर-साल ‘बेरोज़गारों की रिज़र्व फ़ौज’ की तादाद में भारी इज़ाफ़ा हो रहा है। अब यह कैसे मान लिया जाये कि औद्योगिक घराने अपने लाभ बढ़ाने के बजाए अधिक रोज़गार देकर अपने मुनाफ़े की हवस में कमी करेंगे। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या! बक़ौल पॉल क्रुगमैन—जो नोबल इनामयाफ़्ता मशहूर अर्थशास्त्री हैं—मुनाफ़े की एक दिक्कत यह है कि इससे मुनाफ़े की हवस में और ज्यादा आग लग जाती है। अस्तु, रोजगार सब्सिडी से रोज़गार में बढ़ोत्तरी हो न हो लेकिन उद्योगपतियों की ज़रूर पौ बारह होगी।
मनरेगा का एक पहलू यह भी
यह याद करना समीचीन होगा कि, 21 वीं सदी के शुरुवाती वर्षों में जब केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार थी, और बीजेपी सरकार ने 'भारत उदय' (इंडिया शाइनिंग) का भ्रमजाल पूरे मनोयोग से फैलाया था। आर्थिक वृद्धि का गुणगान किया जा रहा था। उस दौरान अगर कुछ चमक (शाइन) रहा था तो पूँजीपतियों और औद्योगिक घरानों की क़िस्मत का तारा चमक रहा था। खेतिहर मजदूर का उदय तो बिलकुल नहीं हो रहा था क्यूंकी इन वर्षों के दौरान खेतिहर मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में प्रति वर्ष का स्तर सिर्फ 0.1 प्रतिशत ही था। लेकिन अगर वर्ष 2005-06 से 2010-11 तक की बात करें तो इस दौरान, कुछ हद तक, बेहतर बातें हुईं। इस दौरान सभी ग्रामीण श्रमिकों बशमूल गैर-कृषि अकुशल मजदूरों (मनरेगा श्रमिकों) की वास्तविक मजदूरी में इज़ाफ़ा हुआ। ख़ास बात तो यह है कि इस दौरान, महिलाओं की वास्तविक मज़दूरी में वृद्धि की रफ़्तार पुरुषों की तुलना में ज़्यादा रही। बेशक, अर्थमितीय दृष्टि से ग्रामीण मजदूरी वृद्धि की इस दर को सिर्फ मनरेगा से मंसूब नहीं कर सकते। लेकिन यह खेतिहर मजदूरों की मज़दूरी और मनरेगा के रिश्ते को दिखाता है।
मनरेगा महज़ रोज़गार सृजन का कार्यक्रम नहीं है। इसके मिलने वाले विभिन्न सामाजिक-आर्थिक लाभों के विभिन्न आयाम हैं। मनरेगा का एक ‘डोमिनो प्रभाव’ यह भी है कि इससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद मिली है। उल्लेखनीय है कि 1995 में बीजिंग में आयोजित चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में यूनीफेम की तत्कालीन निदेशक नॉलिन हॉयज़र ने कहा था कि दुनिया के एक अरब तीस करोड़ लोग नितांत ग़रीब हैं। इनमें महिलाओं कि संख्या 70 फ़ीसदी से भी ज़्यादा है। जबकि औरतें शब-ओ-रोज़ के मश्ग़ले और दुनिया के काम काज के घंटों में दो-तिहाई समय काम करती हैं। लेकिन दुनिया की आमदनी में उसे सिर्फ़ दसवाँ हिस्सा मिलता है। मनरेगा ने हाशिये पर खड़ी औरतों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराया है—भले यह मौक़े कम हों। दूसरी ओर, जाने-माने अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक का मानना है कि नरेगा के जरिये न सिर्फ ग्रामीण गरीबों को भयावह गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली, बल्कि इसी कार्यक्रम की बदौलत वैश्विक आर्थिक संकट के समय भारत पर इसका उस हद तक प्रभाव नहीं पड़ा।
अंत में
मनरेगा के आर्थिक और सामाजिक फ़ायदे को वर्ल्ड बैंक ने भी स्वीकार किया है। विश्व बैंक ने 2009 में अपनी विश्व विकास रिपोर्ट (वर्ल्ड डेव्लपमेंट रिपोर्ट) में नरेगा को "विकास के लिए बाधा" कहा था। लेकिन इस मामले में, 2014 तक आते-आते वर्ल्ड बैंक की राय बदल गयी। नरेगा के बहुआयामी विकास योगदान देखते हुए इसने 2014 की वर्ल्ड डेव्लपमेंट रिपोर्ट में इसे ग्रामीण विकास की ‘दरख़्शां मिसाल’ (‘स्टेलर एक्ज़ैंपल ऑफ रुरल डेव्लपमेंट’) की संज्ञा दी है।
कुल मिल कर, मनरेगा के न तो सामाजिक-आर्थिक लाभ कम हैं और न ही यह अर्थव्यवस्था पर भार है। अगर कमी है तो मौजूदा हुक्मरानों (और देश की अर्थव्यवस्था के मैनेजरों) में राजनीतिक इच्छाशक्ति की। सवाल आर्थिक व्यवहार्यता (इकनॉमिक वायबिलिटि) का नहीं बल्कि प्राथमिकताओं से भटकने का है। अलबत्ता, इतना ज़रूर है कि नरेगा योजना के क्रियान्वयन में कई झोल है जिसे गवर्नेंस के ज़रिये दूर किया जा सकता है। ‘गुड गवर्नेंस’ का कलमा पढ़-पढ़ कर केंद्र में आने वाली मोदी सरकार से उम्मीद थी कि वह गवर्नेंस को दुरुस्त करेगी। लेकिन वह तो आर्थिक भार और राजकोषीय घाटा का बहाना लेकर ग़रीब आदमी की रोज़ी-रोटी पर लात मारने को आमादा है। यही देश का दुर्भाग्य है; और खोटी आर्थिकी भी।
आतिफ़ रब्बानी,
रिसर्च स्कॉलर (अर्थशास्त्र),
सेंटर फॉर द स्टडी इन रीजनल डेव्लपमेंट,
स्कूल ऑफ सोश्ल साइन्सेज़,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली–110067
ई-मेल: csrdian@gmail.com, मोब॰ +91–9711795373