क्रांतिकारी आंदोलन के दस्तावेज और उनके राजनैतिक विचारों का इतिहास
शुभनीत
कौशिक
फ़िलहाल,
जून 2017
हाल के वर्षों में, औपनिवेशिक भारत में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों के इतिहास, उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि, भावी राष्ट्र की उनकी संकल्पना और राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय समाज पर क्रांतिकारी आंदोलन के प्रभाव को लेकर कई पुस्तकें लिखी गईं हैं. शुक्ला सान्याल की किताब क्रांतिकारी आंदोलन को उसकी समग्रता में समझने के इन प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है. शुक्ला सान्याल अपना ध्यान बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के आरंभिक चरण पर केंद्रित करती हैं. उनका अध्ययन-काल, 1905 में बंग-भंग के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन से लेकर प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति तक बंगाल में हुए क्रांतिकारी आंदोलन तक सीमित है. यह वह समय था, जब क्रांतिकारियों ने अपनी राजनैतिक विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए विविध प्रयोग शुरू किए. क्रांतिकारी आंदोलन के इस आरंभिक चरण में किए गए राजनैतिक प्रयोग, न सिर्फ़ इस चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में, बल्कि बाद के क्रांतिकारी आंदोलनों के विकास के बारे में भी हमें अंतर्दृष्टि देते हैं.
जून 2017
हाल के वर्षों में, औपनिवेशिक भारत में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरोध में हुए क्रांतिकारी आंदोलनों के इतिहास, उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि, भावी राष्ट्र की उनकी संकल्पना और राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारतीय समाज पर क्रांतिकारी आंदोलन के प्रभाव को लेकर कई पुस्तकें लिखी गईं हैं. शुक्ला सान्याल की किताब क्रांतिकारी आंदोलन को उसकी समग्रता में समझने के इन प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है. शुक्ला सान्याल अपना ध्यान बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के आरंभिक चरण पर केंद्रित करती हैं. उनका अध्ययन-काल, 1905 में बंग-भंग के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन से लेकर प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति तक बंगाल में हुए क्रांतिकारी आंदोलन तक सीमित है. यह वह समय था, जब क्रांतिकारियों ने अपनी राजनैतिक विचारधारा के प्रचार-प्रसार के लिए विविध प्रयोग शुरू किए. क्रांतिकारी आंदोलन के इस आरंभिक चरण में किए गए राजनैतिक प्रयोग, न सिर्फ़ इस चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में, बल्कि बाद के क्रांतिकारी आंदोलनों के विकास के बारे में भी हमें अंतर्दृष्टि देते हैं.
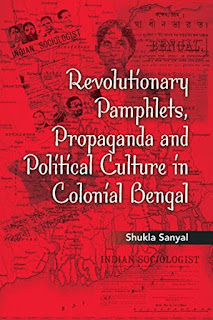 |
रिवोल्यूशनरी
पैम्फलेट्स, प्रोपगेंडा एंड पॉलिटिकल कल्चर इन कॉलोनियल बंगाल, शुक्ला सान्याल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, (2014), पेज 211, कीमत: 695 रुपए.
|
क्रांतिकारियों
की राजनैतिक विचारधारा, उनके मूल्यों, आशाओं और आकांक्षाओं को समझने के लिए, शुक्ला सान्याल क्रांतिकारी संगठनों द्वारा जारी किए गए पैम्फलेटों के
साथ ही, क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए या सहानुभूति रखने
वाले समाचार-पत्रों का भी बखूबी इस्तेमाल बतौर ऐतिहासिक स्रोत करती हैं. साथ ही, वे उस व्यापक राजनैतिक-सांस्कृतिक संसार को समझने की भी कोशिश करती हैं, जिसका ये सभी क्रांतिकारी हिस्सा थे. क्रांतिकारियों के प्रचार-कार्य को
वे एक विमर्श-निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखती हैं,
जिसमें न सिर्फ़ औपनिवेशिक सत्ता और प्राधिकार (अथॉरिटी) के निहितार्थों की गहन चर्चा
की जा रही थी, बल्कि उन अर्थों में बदलाव करते हुए एक ऐसी
अस्मिता को गढ़ने का प्रयास भी किया जा रहा था, जो औपनिवेशिक
अस्मिता से अलग हो (पेज 2). ‘क्रांतिकारी राष्ट्रवादी’ अस्मिता के निर्माण की प्रक्रिया में निजी और सार्वजनिक दायरों के मेल के
साथ ही, भावनात्मक और वैचारिक स्तरों का भी मेल हो रहा था.
साम्राज्यवाद
की वैधता को चुनौती
जनता के
बीच अपने राजनैतिक विचारों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए क्रांतिकारियों ने
समाचारपत्रों और आगे चलकर पैम्फलेटों को एक महत्त्वपूर्ण और शक्तिशाली माध्यम के
रूप में देखा. समाचारपत्र सूचनाएँ और तथ्य मुहैया कराने के साथ-साथ लोकमत का
निर्माण भी करते हैं, इस तथ्य से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू से ही वाकिफ थे. वे यह भी भली-भांति
समझ चुके थे कि लोकमत का प्रतिनिधित्व करने का सीधा अर्थ था - वैधता और प्राधिकार
हासिल करना. उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों को
एकमात्र उपाय के रूप में दिखलाने और अंग्रेज़ी शासन के बरक्स क्रांतिकारी आंदोलन की
वैधता स्थापित करने की कोशिश भी, क्रांतिकारियों ने इन
पत्र-पत्रिकाओं के जरिये की. लोकमत को अपने पक्ष में करने,
उसके निर्माण और नियंत्रण को लेकर क्रांतिकारियों और औपनिवेशिक शासन में संघर्ष
चलता रहा. इस वैचारिक संघर्ष में, क्रांतिकारियों ने युगांतर, संध्या और वंदे मातरम सरीखे समाचारपत्रों के जरिये अपनी
राजनैतिक सोच को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया. युगांतर ने अपने लेखों
में साफ प्रकट होने वाले वैचारिक झुकाव, अपनी राजनैतिक
वाक्पटुता, भाषाई कौशल और ठेठ मुहावरेदार शैली से अपनी एक
अलग ही पहचान बनाई. अपनी इस खास शैली के चलते युगांतर ऐसे रुझान वाले क्रांतिकारी
पत्र-पत्रिकाओं के लिए एक आदर्श बन चुका था.
स्वदेशी
आंदोलन के दौरान ब्रिटिश राज की राजनैतिक वैधता पर सवाल उठने के साथ ही, एक ऐसे राजनैतिक क्षेत्र का भी विकास हुआ, जोकि
अपने स्वभाव में उपनिवेशवादविरोधी था. इस प्रक्रिया ने एक ऐसी नई राजनीतिक भाषा का
विकास किया, जिसमें लोगों से आत्म-रक्षा के लिए हथियार उठाने, प्रतिशोध लेने और पुरुषार्थी बनने का आह्वान किया जा रहा था. स्वदेशी
आंदोलन ने एक ऐसे वैकल्पिक-विमर्श की जमीन भी तैयार की, जो
योरोपीय विचार नियंत्रण से मुक्त था और इसलिए आम भारतीय मानस के न सिर्फ़ बेहद निकट
था, बल्कि उसके अनुरूप भी था. क्रांतिकारी आंदोलन के आरंभिक
चरण के बारे में शुक्ला सान्याल लिखती हैं कि ‘क्रांतिकारी
आंदोलनों से जुड़ी पत्र-पत्रिकाओं में जिस भाषा, जिन सांस्कृतिक
प्रतीकों, कथाओं, छवियों और
व्यक्तित्वों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वह अधिकांशतया
हिंदू धर्म से ली गई होती थी’ (पेज 32). और यह अकारण नहीं था
कि क्रांतिकारी आंदोलन के इस चरण में गैर-हिंदुओं की भागीदारी न के बराबर थी.
युगांतर, संध्या और स्वाधीन भारत के लेखों में और बाद के पैम्फलेटों
में भी अक्सर धार्मिक और पौराणिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे क्रांतिकारियों की गतिविधियों और उनके बलिदानों को एक ‘यज्ञ’ के रूप में देखा जाता था. पर यह बात ज़ोर देकर
कहने की है कि हिंदू धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल के बावजूद क्रांतिकारियों के पैम्फलेटों
में या आमतौर पर उनके लेखन में, गैर-हिंदू समुदायों के प्रति
कोई विरोधभाव नहीं था और उनकी सोच हिंदू पुनरुत्थानवादियों से बिलकुल अलग थी. सान्याल
चेताती हैं कि क्रांतिकारियों के इस सांस्कृतिक अलगाव को अपवर्जन (एक्सक्लूजन) के
रूप में देखना गलत होगा क्योंकि इसी चरण में कई ऐसे पैम्फलेट भी लिखे गए, जिनमें हिंदू-मुस्लिम एकता पर विशेष ज़ोर दिया गया. उनके अनुसार, यह जरूरी नहीं कि एक राजनैतिक उद्देश्य से प्रेरित धार्मिक विमर्श, हमेशा ही सांप्रदायिक हो या दक़ियानूसी और पुरातनवादी हो.
दमन का
प्रतिकार
जाहिर है
कि क्रांतिकारियों के इन प्रयासों से जहाँ साम्राज्यवादी शासन की राजनैतिक वैधता
को खुली चुनौती मिल रही थी, उनके इस उद्यम से औपनिवेशिक सरकार की असहज हो उठना भी बिलकुल स्वाभाविक था.
नतीजतन सरकार ने दमनकारी रवैया अपनाते हुए प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंटने की
पूरी कोशिश की. इस क्रम में औपनिवेशिक सरकार ने अनेक क़ानूनों, मसलन, समाचारपत्र अधिनियम (1908), प्रेस अधिनियम (1910), भारतीय दंड संहिता की धारा
124-ए आदि के जरिये क्रांतिकारी आंदोलन पर हमला बोला. शुक्ला सान्याल
क्रांतिकारियों द्वारा अपनाई गई उन रणनीतियों का भी अध्ययन करती हैं, जिन्हें क्रांतिकारियों ने अपने विचारों के प्रचार-प्रसार हेतु और
औपनिवेशिक सरकार के दमन से निबटने के लिए अपनाया और इस तरह समूची औपनिवेशिक मशीनरी
को धता बताया.
दमनकारी
क़ानूनों की मौजूदगी में जब क्रांतिकारियों के लिए पत्र-पत्रिकाएँ छापना मुश्किल हो
गया, तो उन लोगों ने पैम्फलेट छापने शुरू किए और इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन के
प्रचार-कार्य को रोकने की उन सभी सरकारी कोशिशों को एक हद तक नाकाम साबित कर दिया.
समाचारपत्रों के उलट इन पैम्फलेटों पर नियंत्रण करना, उन्हें
जब्त करना या प्रतिबंधित करना औपनिवेशिक शासन के लिए कभी भी आसान नहीं रहा.
क्योंकि इन पैम्फलेटों में लेखक, प्रकाशक या मुद्रक का नाम
नहीं होता था. ये पैम्फलेट क्रांतिकारियों को सरकार के चंगुल में फंसे बिना, अंग्रेज़ी सरकार को चुनौती देने का अवसर देते थे. पैम्फलेटों के लेखक
अक्सर अंग्रेज़ी राज को बुराई का प्रतीक बताते. और इस तरह
क्रांतिकारियों और सरकार के बीच संघर्ष को अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष का रूप
दे देते थे. सरकार ने पैम्फलेटों के वितरण पर भी अंकुश लगाने की कोशिश की, और इसके लिए इनके लेखकों, प्रकाशकों और वितरकों को
गिरफ़्तार भी किया. पर चूँकि इन पैम्फलेटों की वितरण-प्रणाली
इतनी विकेंद्रित होती थी कि उनके वितरकों को पकड़ना बेहद मुश्किल काम था, इसलिए अंग्रेज सरकार इन पैम्फलेटों के वितरण और प्रसार पर कभी प्रभावी
नियंत्रण नहीं कर पाई.
प्रेरक
विचार
लोगों तक
राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने के लिए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी रचनाओं में (और
राष्ट्रीय आंदोलन में भी), जिस ऐतिहासिक अतीत को गढ़ा जा रहा था, उसके ‘ऐतिहासिक आख्यान’ में जितनी वास्तविक ऐतिहासिक
घटनाएँ होती थीं, उससे कहीं ज्यादे हिस्सा मिथक और स्मृतियों
का होता था. मिथक से भरे इन्हीं आख्यानों के जरिये राष्ट्र के अतीत और वर्तमान के
बीच प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी. पर ध्यान रखना होगा कि इस
दौरान पुरानी अवधारणाओं और प्रत्ययों को अपनाया जरूर जा रहा था, पर जस-का-तस नहीं. उनके अर्थों में आरंभिक 20वीं सदी की जरूरतों को ध्यान
में रखते हुए जरूरी फेरबदल भी किए जा रहे थे. राष्ट्र और राष्ट्रीय समुदायों से
जुड़े ऐतिहासिक आख्यानों और ‘आविष्कृत’
परम्पराओं के ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए एरिक हाब्सबाम और टेरेंस रेंजर द्वारा
संपादित किताब द इन्वेंशन ऑफ ट्रेडीशन (1983) में संकलित लेख भी पढ़े जाने
चाहिए.
शुक्ला
सान्याल के अनुसार, क्रांतिकारी आंदोलन के इस आरंभिक चरण पर तीन भारतीय विचारकों, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद और अरविंद
घोष का प्रभाव उल्लेखनीय था. बंकिम ने अपने लेखन में राष्ट्र-निर्माण के लिए इतिहास
पर ज़ोर दिया था. पर ख़ुद बंकिम का ऐतिहासिक लेखन औपनिवेशिक इतिहासलेखन से गहरे
प्रभावित था. औपनिवेशिक इतिहासकारों, मसलन जेम्स मिल द्वारा
किए गए काल-विभाजन से; जिसमें भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बाँटा गया और मध्यकाल को पतन के काल के रूप
में दिखाया गया, बंकिम को कोई आपत्ति नहीं थी. बंकिम ने
भारतीय राष्ट्रवाद को राष्ट्रीय अस्मिता गढ़ने के लिए सांस्कृतिक प्रतीक, छवियाँ और नारे जरूर दिये, पर साथ ही इन प्रतीकों
ने भारतीय राष्ट्रवाद की ऐसी छवि विकसित की, जिसकी जड़ें हिंदू
धार्मिक परंपरा में कहीं गहरे समाये हुए थीं (पेज 66). बंकिम ने ‘अनुशीलन’ का सिद्धांत भी दिया,
जिसके अनुसार स्वतन्त्रता हासिल करने के लिए भारतीयों को शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना
जरूरी था. क्रांतिकारी आंदोलन को प्रभावित करने वाले दूसरे प्रमुख विचारक स्वामी
विवेकानंद का ज़ोर समाज-सेवा पर था. विवेकानंद ने भारतीयों से ‘पुरुषार्थी’ बनने का आह्वान किया. उनके अनुसार
धार्मिक क्षेत्र में देश को पुनर्जीवन मिलने के बाद ही, देश
के राजनैतिक-आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र में कोई बदलाव संभव था. जबकि अरविंद घोष के
लिए राजनैतिक स्वतन्त्रता देश के पुनरुद्धार के लिए पहली आवश्यक शर्त थी. इन तीनों
ही विचारकों ने क्रांतिकारी आंदोलन और क्रांतिकारियों की विचारधारा पर अमिट प्रभाव
छोड़ा.
सखाराम
गणेश देउस्कर द्वारा रचित देशेर कथा (जिसके 1904-08 के दौरान बांग्ला में पाँच
संस्करण छपे और हिन्दी में भी जिस पुस्तक के एकाधिक अनुवाद हुए) जैसी अर्थशास्त्र
पर लिखी किताबों, इतिहास, राजनीति और धार्मिक पुस्तकों के अलावा, क्रांतिकारियों के अपने दैनंदिन जीवन के निजी अनुभवों ने भी उन्हें
क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा दी. वाल्तेयर,
रूसो और मैझिनी सरीखे पश्चिमी विचारकों और विभूतियों ने भी क्रांतिकारी आंदोलन की
विचारधारा को प्रभावित किया. साथ ही, वैश्विक घटनाओं ने भी, मसलन रूस-जापान युद्ध (1905) और आगे चलकर रूसी क्रांति ने भी क्रांतिकारी
आंदोलन पर प्रभाव डाला. पराधीन राष्ट्र में जीने को,
क्रांतिकारियों द्वारा न सिर्फ़ अपने आत्म-सम्मान को खोने,
बल्कि अपनी अस्मिता को भी खो देने के रूप में देखा गया.
पुरूषवादी
आख्यान
उन्नीसवीं
सदी के दौरान ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में पहली बार
प्रकाशित गीत वंदे मातरम के जरिये, भारत माता की
संकल्पना की. मातृदेवी से प्रेरित यह बेहद शक्तिशाली संकल्पना न सिर्फ़ क्रांतिकारी
आंदोलनों में बल्कि समूचे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रेरणादायी विचार के रूप
में जरूर उभरी, पर इसने गैर-हिंदुओं के लिए ख़ासकर मुस्लिमों
के लिए असहजता भी पैदा की. चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपनी कूची से बंकिम की
अमूर्त संकल्पना को एक मूर्त और आत्मीय रूप दिया. स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी
बंग-भंग का विरोध करते हुए समूची बंगाली जनता से ‘बंग-माता’ के सम्मान की रक्षा की गुहार की गई. पर इस चरण के क्रांतिकारी पैम्फलेटों
के विश्लेषण से सान्याल दिखाती हैं कि जब भारत माता और उसके संतानों की चर्चा की
जा रही होती थी, तो वह अक्सर पुत्रों तक ही सीमित होती थी (पेज
59). क्रांतिकारी आंदोलन के इस आरंभिक चरण में आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को
लेकर एक चुप्पी थी.
‘बंधुत्व’ की जिस अवधारणा की चर्चा क्रांतिकारी पैम्फलेटों में होती थी, वह भी पुरूषों तक ही सीमित थी. सान्याल के अनुसार, भारत
माता की ‘संतान’ से भी तात्पर्य अक्सर
पुत्रों से ही होता था, पुत्रियों से नहीं (पेज 177-8). भारतीय
पुरूष का यह दायित्व समझा जाता था कि वह भारत माता के साथ ही, भारतीय महिलाओं यानी अपनी माताओं, बहनों और बेटियों
के सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा अंग्रेज़ों से करे. क्रांतिकारी आंदोलन ने अपने
आरंभिक चरण में, आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के
प्रश्न पर गंभीरता से विचार नहीं किया, पर राजनैतिक
गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी का कभी विरोध भी नहीं किया. अपने इस चरण में
क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका मुख्यतः बस यही थी कि वे अपने पुत्रों
और भाईयों को देशहित में समर्पित कर दें और इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थन
करें (पेज 180). महिलाओं की भागीदारी के प्रश्न पर क्रांतिकारी आंदोलन की यह
चुप्पी आंदोलन के अगले चरण में जाकर ही ख़त्म हो सकी, जब
महिलाओं ने क्रांतिकारी आंदोलन में बढ़-चढ़कर भागीदारी की.
हिंसा का
सवाल
क्रांतिकारी
आंदोलन में हिंसा का प्रश्न एक अन्य महत्त्वपूर्ण विषय है, जिसकी चर्चा शुक्ला सान्याल अपनी इस पुस्तक में करती हैं. उनका तर्क है
कि बहुधा क्रांतिकारी आंदोलनों ने अपनी हिंसात्मक कार्यवाहियों को अपने
प्रचार-कार्य (प्रोपगेंडा) का ही एक हिस्सा समझा और उसे वैध ठहराने का प्रयास किया.
हिंसा के प्रश्न पर विचार करते हुए शुक्ला सान्याल तीन पक्षों यानी एक पक्ष जो
हिंसा प्रायोजित कर रहा है, दूसरा पक्ष जो हिंसा का शिकार हो
रहा है, और तीसरा पक्ष जो हिंसा का प्रत्यक्षदर्शी है, को ध्यान में रखने की सलाह देती हैं. वे दिखाती हैं कि अपने आरंभिक चरण
में भी क्रांतिकारियों को यह एहसास हो चला था कि हिंसक गतिविधियों से औपनिवेशिक
शासन की अजेयता की छवि को जरूर तोड़ा जा सकता है, पर इससे
किसी दीर्घकालीन उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती थी. क्योंकि अंततः क्रांतिकारी
आंदोलन का असल उद्देश्य तो उपनिवेशवाद के खिलाफ़ लंबी लड़ाई के लिए देश को तैयार
करना था. इस चरण में क्रांतिकारी आंदोलनों ने अपनी हिंसक गतिविधियों को वैध ठहराने
के लिए उन्हें ‘दैवीय इच्छा’ का नतीजा
तक बताया.
भाषाई सीमा
पैम्फलेटों
की वैचारिक सीमा का एक दूसरा पहलू था उनमें इस्तेमाल होने वाली भाषा का. यह भाषा
बगैर किसी अपवाद के साधु बांग्ला (संस्कृतप्रधान बांग्ला) थी. पैम्फलेटों
में इस्तेमाल होने वाले धार्मिक-सांस्कृतिक प्रतीक ही नहीं, उनकी भाषा भी यह जतला देती है कि इस आरंभिक चरण में क्रांतिकारी आंदोलन
जिस वर्ग को लक्षित कर रहा था, वह था शहरों में रहने वाला
उच्च जाति का शिक्षित युवा वर्ग. अपने आरंभिक चरण में ख़ुद क्रांतिकारी आंदोलन के
अधिकांश सदस्य कुलीन वर्ग से आते थे और उस समय के यानी आरंभिक 20वीं सदी के बंगाल
के राजनैतिक वातावरण को देखते हुए यह अस्वाभाविक नहीं था कि उनका लक्ष्य शहर में
रहने वाले शिक्षित युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना था. और यह भी कि इस चरण में
आम लोगों से उनकी भाषा में राजनैतिक संवाद स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया
या शायद कुलीन वर्ग से आने वाले क्रांतिकारी इसकी जरूरत को अधिक गहराई से नहीं समझ
सके. बाद के चरणों में ही क्रांतिकारी आंदोलन अपने संगठन में अधिक समावेशी बन सका.
साथ ही, समाजवाद के प्रभाव से, बाद के
क्रांतिकारी आंदोलनों में, धार्मिक प्रतीकों वाली भाषा की
जगह, एक अधिक धर्मनिरपेक्ष और समावेशी भाषा का प्रयोग किया
जाने लगा. शुक्ला सान्याल की यह पुस्तक क्रांतिकारी आंदोलन में दिलचस्पी रखने
वालों के साथ-साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में रूचि रखने वाले हर
व्यक्ति के लिए अनिवार्य रूप से पठनीय है.
हमें अब इस परिपाटी पर ही चलना पड़ेगा
जवाब देंहटाएं